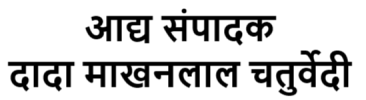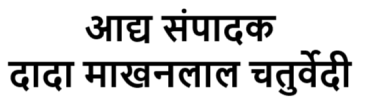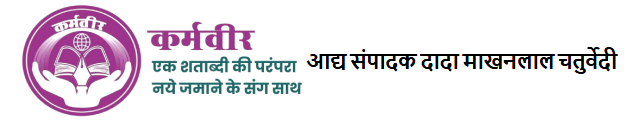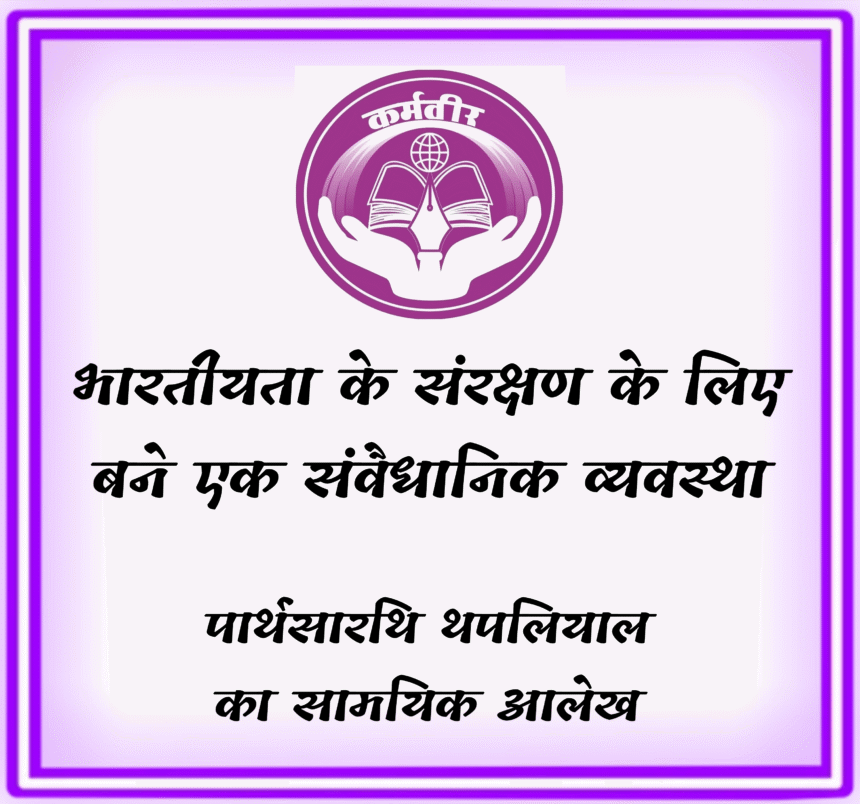स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने लोकतंत्र को अपना आधार बनाकर विविधताओं से भरे समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। परंतु विडंबना यह है कि जिस लोकतंत्र से राष्ट्रीय एकता और नागरिक समरसता की रक्षा अपेक्षित थी, वही अनेक अवसरों पर राजनीतिक स्वार्थों का उपकरण बनता दिखाई देता है। कभी हिंदू-मुस्लिम दंगे, कभी क्षेत्रीय स्वायत्तता के नाम पर आंदोलन, कभी अलग देश की मांग, तो कभी जातीय आरक्षण के प्रश्न पर सामाजिक विभाजन, ये सभी प्रवृत्तियाँ इस ओर संकेत करती हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया केवल चुनाव तक सीमित होकर रह गई है, जबकि उसका नैतिक उद्देश्य पीछे छूटता जा रहा है।
लोकतांत्रिक पदों पर आसीन व्यक्ति संविधान की शपथ लेते समय सत्यनिष्ठा और राष्ट्रनिष्ठा का संकल्प करते हैं, पर व्यवहार में अक्सर यह शपथ औपचारिकता बनकर रह जाती है। वोट-बैंक की राजनीति ने जातियों और समुदायों के बीच विद्वेष को हवा दी है। शिक्षा और नौकरियों में योग्यता के स्थान पर पहचान आधारित प्राथमिकताओं ने असंतोष को जन्म दिया है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र पर आघात है। जब शासन व्यवस्था स्वयं भेदभाव और पक्षपात को प्रोत्साहित करने लगे, तब लोकतंत्र अपनी मूल आत्मा खो देता है।
इसके साथ ही भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता को क्षीण करने वाले राजनीतिक षड्यंत्र भी सामने आते हैं। परंपराओं को “पिछड़ापन” बताकर, राष्ट्रीय प्रतीकों को विवादास्पद बनाकर, भारतीय संस्कृति को अपमानित कर और इतिहास को खंडित दृष्टि से प्रस्तुत कर समाज को मानसिक रूप से विभाजित किया जा रहा है। यह स्थिति केवल सामाजिक संकट नहीं, बल्कि सभ्यतागत संकट है। प्रश्न यह है कि क्या केवल वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचा इन सभी कुसंगतियों का समाधान कर सकता है? अनुभव बताता है कि राजनीतिक दल स्वयं इन समस्याओं का हिस्सा बन चुके हैं, अतः उनसे समाधान की अपेक्षा करना यथार्थवादी नहीं प्रतीत होता।
इसी संदर्भ में “राष्ट्रप्रथम ध्येय आयोग” जैसी संवैधानिक संस्था की परिकल्पना विचारणीय हो जाती है। यदि हाईकोर्ट के न्यायाधीश स्तर का कोई व्यक्ति, अथवा किसी दलीय विचार से हटकर कोई विधिवेता और सांस्कृतिक चेतना युक्त राजपुरुष की अध्यक्षता में आयोग या कोई परिषद की स्थापना, (संसद द्वारा अधिनियम बनाकर), राष्ट्रपति करे, जिसे संविधान द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त हों, तो वह राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की कसौटी पर नीतियों और आचरण का मूल्यांकन कर सकता है। इस आयोग के चार बाह्य सदस्य हों जिनमें से एक सर्वोच्च न्यायालय का नामित जज, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और दलीय राजनीति से दूर, एक राष्ट्र चिंतक। यह आयोग/परिषद न केवल सरकारी निर्णयों की समीक्षा करेगा, बल्कि उन प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाएगा जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती हैं, चाहे वे सांप्रदायिक हों, क्षेत्रीय हों या जातीय। यह व्यवस्था अपनी सलाह सीधे राष्ट्रपति को दे।
इस प्रकार का आयोग/परिषद लोकतंत्र का विकल्प नहीं, बल्कि उसका नैतिक संरक्षक होगा। जैसे चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करता है, वैसे ही “राष्ट्र प्रथम ध्येय आयोग” शासन और राजनीति को यह स्मरण कराएगा कि उनका अंतिम लक्ष्य सत्ता नहीं, राष्ट्र है। यह आयोग यह भी देख सकेगा कि आरक्षण, स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की अति स्वतंत्रता, द्वेषपूर्ण सामाजिक/ धार्मिक आंदोलन या विशेष अधिकार जैसे निर्णय सामाजिक संतुलन को तोड़ने का साधन न बनें, बल्कि न्याय और समरसता के उपकरण रहें।
निस्संदेह, ऐसी संस्था की स्थापना में चुनौतियाँ होंगी। इसके अधिकारों की सीमाएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप से इसकी स्वतंत्रता और इसके निर्णयों की वैधता, ये सभी प्रश्न गंभीर विमर्श मांगते हैं। परंतु जब राष्ट्र बार-बार विभाजनकारी राजनीति का शिकार हो रहा हो, तब किसी उच्च नैतिक प्राधिकरण की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।
समय की आवश्यकता है कि लोकतंत्र को केवल बहुमत का गणित न रहने दिया जाए, बल्कि उसे राष्ट्रधर्म से जोड़ा जाए। जो यह सुनिश्चित करे कि नीति, सत्ता और राजनीति का अंतिम लक्ष्य भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता हो। तभी लोकतंत्र अपने वास्तविक अर्थ में जनता और राष्ट्र दोनों की रक्षा कर सकेगा।

पार्थसारथि थपलियाल
(लेखक भारतीय संस्कृति सम्मान अभियान के संयोजक,मीडियाकर्मी और स्वतंत्र लेखक हैं।)