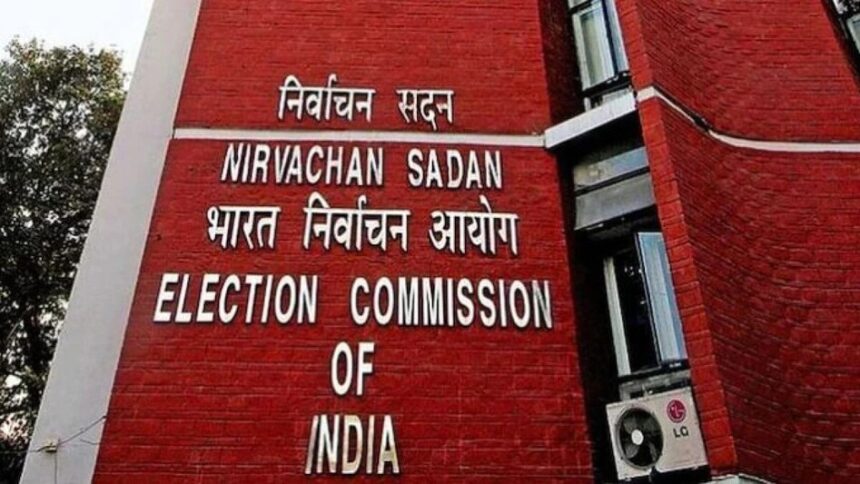इन दिनों ‘एक देश,एक चुनाव’ का मुद्दा गर्म है।इस संबंध में बहस और चर्चाएं तो पहले से चल रही हैं, लेकिन लोकसभा में तत्संबंधी 129 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत होते ही बहस तेज हो गई है।
लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए व्यापक विचार विमर्श आवश्यक भी है और शुभ लक्षण भी।
एक पक्ष को ‘एक देश, एक चुनाव’ व्यवस्था में सिर्फ अच्छाइयां नजर आ रही हैं, तो दूसरे पक्ष को सिर्फ खामियां। उल्लेखनीय यह है कि जिस पक्ष,यानी आम आदमी की सुविधा के नाम पर यह संशोधन प्रस्तावित है,वह कहीं भी बहस में शामिल नहीं है।
प्रथम दृष्टया ‘एक देश,एक चुनाव’ का विचार आकर्षक लगता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी इसके पक्ष में लंबी-चौड़ी रिपोर्ट दी है।
आजादी के बाद के पहले चार चुनाव एक साथ ही संपन्न हुए थे। वह दौर एक ही पार्टी के प्रभुत्व का था। 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय पूर्व भंग होने की वजह से यह क्रम टूट गया।
अब तो लगभग साल भर ही या तो किसी राज्य में चुनाव चल रहे होते हैं अथवा उनकी तैयारी चल रही होती है।
विधेयक के समर्थकों का कहना है कि बार-बार चुनावों की वजह से देश पर पड़ने वाला वित्तीय वोझ अंततः आम लोगों के कंधों पर ही पड़ता है। चुनावी व्यस्तता की वजह से अधिकारियों का ध्यान अपने मूल कार्यों से भटकता है। देश के किसी न किसी हिस्से में आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने की वजह से नीतिगत और नियमित प्रशासकीय गतिविधियों में व्यवधान पड़ता है। इसके अलावा नीति नियंताओं की चुनावी व्यस्तता की वजह से विकास संबंधी गतिविधियों की निरंतरता भी बाधित होती है।
इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो बार-बार चुनावों की झंझट से देश को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है।
प्रस्तावित ‘एक देश,एक चुनाव’ व्यवस्था के विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं,उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारी संसदीय प्रणाली, जिसमें सरकारों के लिए बहुमत बनाए रखना अनिवार्य है।अल्पमत में आते ही सरकार गिर जाती है और पुनः सरकार गठित करने के लिए चुनाव ही एकमात्र विकल्प बचता है।
लोकतांत्रिक-संसदीय प्रणाली के समर्थक कहते हैं कि यह भले ही श्रमसाध्य और खर्चीला हो लेकिन लोकतंत्र में जनादेश ही निर्णायक होता है,जिसके लिए चुनाव ही एकमात्र विकल्प है।
एक साथ चुनावों के लिए कोविंद समिति ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार निर्धारित तिथि पर जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा हो,उसे बढ़ा दिया जाए और जिनका कार्यकाल बाद में समाप्त हो रहा हो उनका कार्यकाल घटा दिया जाए।
विपक्षी इस विचार को सिरे से खारिज ही नहीं कर रहे,अपितु इसे देश के संघीय स्वरूप के खिलाफ और अलोकतांत्रिक भी करार दे रहे हैं।
विपक्ष का यह भी कहना है कि लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय शासन संस्थाओं के मुद्दे अलग-अलग होते हैं, अतः मतदान का पैटर्न भी अलग-अलग होता है। एक साथ मतदान के लिए बाध्य करना मतदाता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
गठबंधन सरकारों के इस दौर में कौन सी सरकार कब गिर जाए, कहा नहीं जा सकता। एक देश,एक चुनाव व्यवस्था लागू होने के बाद यदि कोई राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर गिर जाती है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस बारे में भी स्पष्टता होनी चाहिए।
एक और मुद्दा है जिस पर सवाल उठना लाज़िमी है। जब निर्वाचन आयोग एक ही राज्य के चुनाव कई-कई चरणों में करवाता है, तो पूरे देश के चुनाव एक साथ करवा पाना क्या उसके लिए संभव होगा?
हो सकता है,संयुक्त संसदीय समिति इन बिंदुओं पर विचार करे।
इस पूरे विचार-विमर्श में जिस पक्ष की आवाज़ सिरे से नदारद है, वह है ‘जनपक्ष’, जिसकी सुविधा और भलाई के नाम पर यह सारी कवायद की जा रही है।
विधि आयोग अथवा संयुक्त संसदीय समिति विषय विशेषज्ञों का समूह हो सकता है,लेकिन पिछले 75 वर्षों में अनेक बार अपनी राजनीतिक समझ और निर्णय क्षमता से सभी को चमत्कृत करने वाली आम जनता प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में क्या सोचती है,इस पर ध्यान दिया जाना भी जरूरी है।
आम लोग भली-भांति जानते हैं कि तमाम खामियों के बावजूद लोकतांत्रिक-संसदीय शासन प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ है। आम लोग यह भी जानते हैं कि प्रचलित प्रणाली की खामियों का फायदा राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों के अनैतिक व्यवहार पर चौबारों-चौपालों पर नाराजगी भी प्रकट होती है, लेकिन नाराजगी के यह स्वर असंगठित होने की वजह से नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर रह जाते हैं।
मोटे तौर पर सभी चाहते हैं कि निरंतर चलने वाले चुनावों से राहत मिले। ‘एक देश,एक चुनाव’ इसका बेहतर विकल्प हो सकता है।
जनपक्ष यह भी चाहता है कि क्यों ना प्रस्तावित व्यवस्था को व्यापक चुनाव सुधारों के साथ लागू किया जाए।
जनपक्ष जिस मुद्दे को लेकर सर्वाधिक चिंतित है वह है दल-बदल और हॉर्स ट्रेडिंग की प्रवृत्ति।
हाॅर्स ट्रेडिंग, दल बदल और ‘आया राम-गया राम’ की प्रवृत्ति भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की वह बुराईयां हैं जिनके कारण लोकतंत्र की आत्मा घायल होती है।
यह हास्यास्पद है कि किसी व्यक्ति की आस्था न केवल रातों-रात बदल जाए अपितु दूसरे ही दिन वह पूरी ठसक के साथ अपनी परिवर्तित आस्था के अवलंबरदारों का लाडला भी बन जाए।
निर्वाचित प्रतिनिधि दल बदल कानून की व्यवस्थाओं का फायदा भी अंतरात्मा की आवाज के नाम पर उठाते रहते हैं। इस कानून के अनुसार यदि अंतरात्मा की आवाज एक निश्चित संख्या में है, तो इसे दल का विभाजन मान लिया जाता है और सदस्यता बची रहती है।
जनपक्ष चाहता है कि राजनीतिज्ञ अपनी अंतरात्मा की पुकार पर आस्था बदलें लेकिन जिस नई विचारधारा के प्रति विश्वास प्रकट कर रहे हैं, कम से कम अगले चुनाव तक उसके मूलभूत तत्वों को आत्मसात तो करें। नए दल के आचार-विचारों के अनुरूप अपने आपको ढालें। फिर पूरी मानसिक तैयारी के साथ चुनावी समर में कूदें। इससे आम जनता में नेतृत्व के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा।
बाकायदा कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि दल- बदल अथवा दल विभाजन में शामिल जनप्रतिनिधि अगले एक चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हों।
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, यदि सरकार कार्यकाल पूरा किए बगैर गिर जाती है,तब क्या होगा? प्रस्तावित विधेयक में संभवतः यह प्रावधान है कि सदन के शेष समय के लिए चुनाव होंगे। यदि फिर भी बहुमत वाली सरकार नहीं बन सकी, तब क्या होगा?
विपक्षियों को आशंका है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होगा जो अंततः अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का ही शासन होगा।
इस आशंका को दूर करने के लिए क्या यह प्रावधान नहीं जोड़ा जा सकता कि ऐसी स्थिति में शेष समय के लिए सर्वदलीय सरकार का गठन होगा। एक ऐसी सरकार जिसमें प्रत्येक दल को उसकी सदस्य संख्या के अनुसार मंत्री पद मिलेंगे।
अलग-अलग वैचारिक धरातल पर खड़े राजनीतिक दलों के लिए यह एक जटिल स्थिति होगी,लेकिन पुनः चुनाव में जाने अथवा राष्ट्रपति शासन के रूप में केंद्र के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप जैसी आशंकाओं को दूर करने के लिए यही एक बेहतर समाधान हो सकता है।
हर राजनीतिक दल अंततः जनसेवा के लिए ही तो सरकार में आना चाहता है। क्या आम मतदाता राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा नहीं रख सकता कि वह सर्वदलीय सरकार गठित होने की स्थिति में अगले चुनावों तक अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को परे रखते हुए जनसेवा करें।
यकीन मानिए जब तक अंतरात्मा की तथाकथित दखलंदाजी राजनीतिक दलों में रहेगी तब तक गठबंधन की सरकारें बनती-बिगड़ती रहेंगी।
यह भी सुनिश्चित है कि जब तक ‘एक देश,एक चुनाव’ की व्यवस्था व्यापक चुनाव सुधारों और सुस्पष्ट निर्दोष कानूनी प्रावधानों के साथ नहीं अपनाई जाएगी, इसका हश्र भी वही होगा जो दल-बदल विरोधी कानून का हुआ है। निहित स्वार्थ के वशीभूत विशेषज्ञ और लाभार्थी इस व्यवस्था में भी अपने मनोनुकूल प्रावधान निकाल ही लेंगे।
*अरविन्द श्रीधर