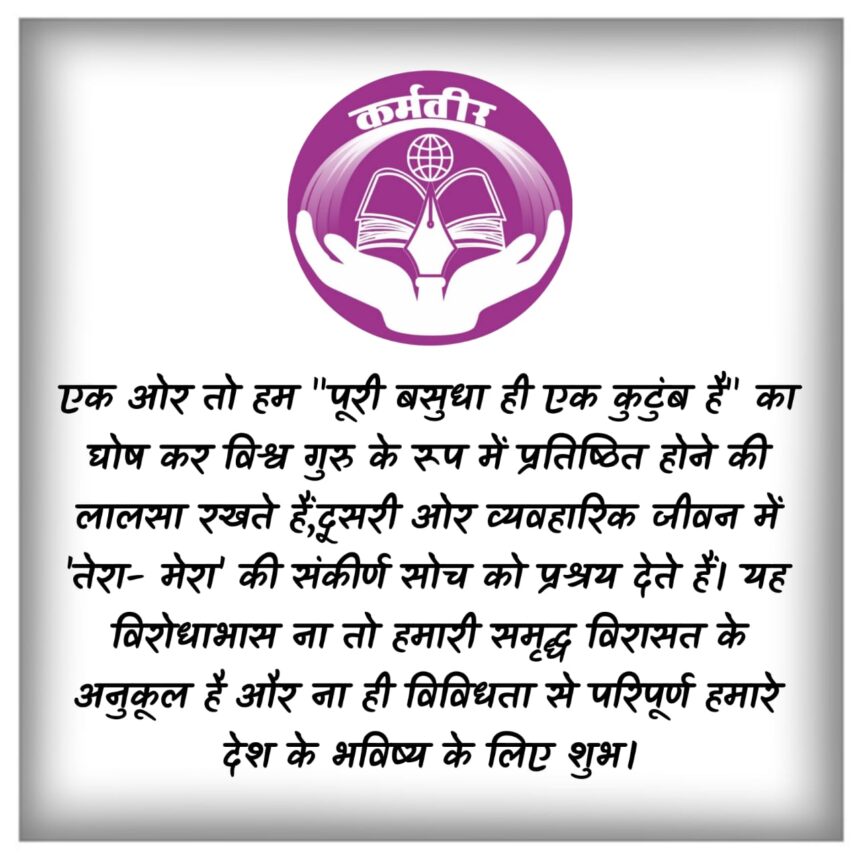विचार विनिमय की स्वस्थ परंपरा हमारी संस्कृति का प्रमुख आधार रही है। मुद्दा चाहे सामाजिक- सार्वजनिक जीवन से संबंधित हो अथवा ज्ञान के गूढ़ रहस्यों से संबंधित मत-मतांतरों का,अंतिम निर्णय हमेशा विचार-विनिमय अथवा शास्त्रार्थ से ही होते रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जब धुर विरोधी पक्षों में शास्त्रार्थ के उपरांत आम सहमति बनी है।
यदि आम सहमति नहीं भी बन सकी तो भी असहमति का सम्मान हमारा एक उच्च मानवीय गुण रहा है।
केवल मैं और मेरा विचार ही सही है, बाकी सब अस्वीकार्य है, ऐसी संकीर्ण सोच हमारी संस्कृति में कभी भी स्वीकार्य नहीं रही।
तेरे-मेरे का विचार किए बगैर गुणी लोगों की सराहना और प्रोत्साहन तथा समाज विरोधी तत्वों की भर्त्सना भी हमारे समाज का चरित्र रहा है। कदाचित इसीलिए हमारे देश में अनेक मत-मतांतर,धर्म-संप्रदाय,रीति-रिवाज सहित
तमाम विविधताएं फल फूल सकीं।
आज का दौर इसके ठीक उलट है। अब चलन है ऊंची आवाज का और अपनी बात पर अड़े रहने का। किसी और का पक्ष सुनने का धैर्य अब प्रायः दुर्लभ होता जा रहा है।आम सहमति अथवा असहमति का सम्मान तो जैसे दूर की कौड़ी हो गई है।
तेरा-मेरा की यही संकीर्ण सोच प्रतिभाओं को सम्मानित-प्रोत्साहित करने के सिलसिले में भी देखने में आती है।
इस बीमारी ने समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार से लगाकर देश की सर्वोच्च संस्था संसद तक को अपनी चपेट में ले लिया है।
सोशल मीडिया की असीमित पहुंच के इस दौर में सही- गलत,उचित-अनुचित अथवा सराहना-भर्त्सना का फैसला अब तथ्यों, विचार-विनिमय अथवा गुण-दोषों के आधार पर नहीं अपितु तेरे-मेरे के आधार पर होने लगा है।
यह और भी बड़ी विडंबना है कि ‘तेरे-मेरे’ की इस संकीर्ण सोच को वैचारिक प्रतिबद्धता का नाम दिया जा रहा है। तथाकथित वैचारिक प्रतिबद्धता जनित अंध समर्थन अथवा अंध विरोध से समाज और देश का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है।
वैचारिक पक्षाघात की इस बीमारी से समाज का हर वर्ग ग्रसित है, लेकिन कहा जा सकता है कि राजनीति
ने इस मामले में बढ़त बनाई हुई है।
कहने को तो हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव को भी मान्यता नहीं देता, लेकिन कौन नहीं जानता कि देश की राजनीति का ताना-बाना इन्हीं दोनों मुद्दों पर ही बुना हुआ है। राजनीतिक फैसले लेते समय तेरा धर्म-मेरा धर्म,तेरी जाति-मेरी जाति ही सबसे बड़ा आधार बन गया है। किसकी मजाल है जो इस चक्र से बाहर निकलने के बारे में सोच सके।
ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ऐसी स्थिति थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब समाज ने अपने जागरूक होने का परिचय देते हुए जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश हित में सोचा है।
प्रखर समाजवादी एवं संविधान वेत्ता हरि विष्णु कामथ का उदाहरण ही देखिए। श्री कामथ होशंगाबाद-नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए थे,जबकि उनकी जाति का शायद ही एकाध मतदाता इन जिलों में हो।
हाॅलांकि यह उस दौर की बात है जब नेता का नैतिक पक्ष अत्यंत सबल हुआ करता था और आम जनता सहज ही अपने नेता का अनुसरण करती थी। राजनीतिक स्वार्थ बस धर्म और जाति की विभाजन रेखाएं शनै शनै इतनी गहरी होती जा रही हैं कि अब किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसे पार करना लगभग असंभव हो गया है।
तेरा-मेरा का यह भाव केवल चुनाव के वक्त टिकट वितरण तक ही सीमित नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए तो अपराधी भी तेरा-मेरा हो गया है।
राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को देखिए, किस बेहयाई के साथ अपने दल के अपराधियों का बचाव, दूसरे दल के अपराधियों के बारे में जोर-जोर से बोल कर करते हैं। इन प्रवक्ताओं के श्री मुख से अपने दल के भ्रष्टाचारी अथवा बलात्कारियों के ख़िलाफ़ एक बोल भी नहीं फूटता। आप कितना भी पूछिए, वह दूसरे दल के अपराधियों की सूची ही गिनाएगा। कमाल है। अपराधी भी तेरा-मेरा।
कोई कुछ भी कहे,लेकिन यह खुला रहस्य है कि आजकल कोई भी निर्णय लेते समय धार्मिक और जातिगत हित साधन ही प्रमुख आधार हैं।अब ऐसा करते हुए अनायास यदि देश हित भी सध जाए तो अच्छी बात है।
दुखद तो यह है कि राजनीति ने महापुरुषों को भी जाति और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। समाज सुधारकों और अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले महापुरुषों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज़ादी के बाद उनकी हैसियत सिर्फ अपनी जाति के नेता की ही बचेगी। राष्ट्र नायक के रूप में तो उन्हें मजबूरी बस ही याद किया जाएगा।
अब जरा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर दृष्टिपात कर लेते हैं। राजनीति का तो जैसे नैतिकता के साथ तलाक ही हो चुका है,पर मीडिया तो आम आदमी की आवाज़ बनने का दम भरता है। क्या ऐसा है? निश्चित रूप से नहीं। इक्का- दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो मीडिया जगत में कहीं अधिक ‘तेरा-मेरा’ नज़र आता है। या तो अंध समर्थन अथवा अंध विरोध। नीर क्षीर विवेक का नितांत अभाव। मीडिया ट्रायल के चलन ने तो जैसे एक नई व्यवस्था ही बना डाली। ‘मेरे’ के अंध समर्थन में चुप्पी और ‘तेरे’ के अंध विरोध में अति मुखरता एक आम चलन है।
एक ओर तो हम “पूरी बसुधा ही एक कुटुंब है” का घोष कर विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने की लालसा रखते हैं,दूसरी ओर व्यवहारिक जीवन में ‘तेरा- मेरा’ की संकीर्ण सोच को प्रश्रय देते हैं। यह विरोधाभास ना तो हमारी समृद्ध विरासत के अनुकूल है और ना ही विविधता से परिपूर्ण हमारे देश के भविष्य के लिए शुभ।
देश और देश में स्वस्थ लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए इस संकीर्ण सोच से बाहर निकलना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हम अपने आपको आदिम कबीलाई युग में पाएं और सारे फैसले संख्या बल, बाहुबल और ऊंची आवाज़ के आधार पर ही होने लगें।
*अरविन्द श्रीधर