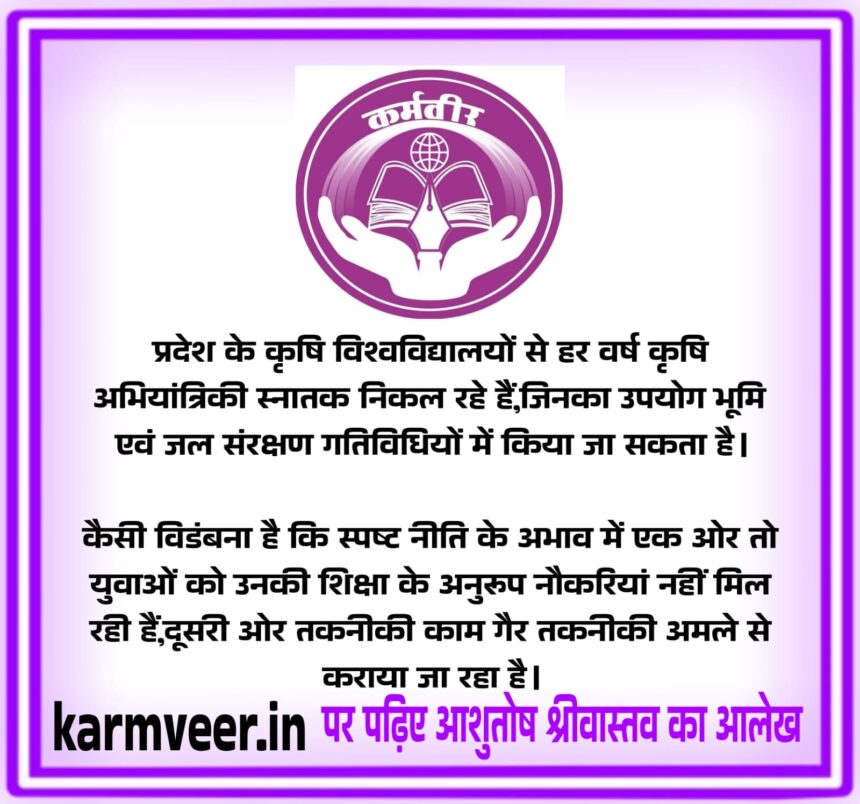विश्व के अनेक देशों में जल संकट की आहट सुनाई दे रही है। भारत में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। देश के अनेक शहरों में भूजल स्रोत सूख रहे हैं। झीलें और तालाब या तो सूख चुके हैं अथवा अंतिम सांसें गिन रहे हैं। गुरुग्राम जैसे शहरों में तो 1000 फीट गहराई पर भी भूमिगत जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
पानी की कमी का सर्वाधिक असर कृषि पर पड़ता है,जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
देहरादून स्थित केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न शोधों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में समा जाता है,कुछ भाग वाष्पीकृत हो जाता है एवं लगभग 50% जल सतह पर व्यर्थ बह जाता है। इसे ‘रनआफ’ कहते हैं। रनआफ के कारण पानी तो व्यर्थ बहता ही है,अपने साथ खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी बहा कर ले जाता है। इसके कारण तालाबों एवं बांधो में गाद भी जमा होती है, जिससे उनकी जल संग्रहण क्षमता कम होती जाती है।
भारत में प्रारंभिक तौर पर भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यों को जिस गंभीरता से प्रारंभ किया गया था, कालांतर में उनमें शिथिलता आती गई। विशेषज्ञों का कहना है कि सिंचाई कार्यों के लिए जल संसाधन विभाग पर निर्भरता इसके मूल में है, जबकि भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो के माध्यम से भी इसे किया जा सकता था।
मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में यदि देखा जाए तो वर्ष 1981 में कृषि विभाग के अंतर्गत 81 भूमि एवं जल संरक्षण उप संभाग स्थापित कर इन्हें भूमि एवं जल संरक्षण गतिविधियों के क्रियान्वयन का दायित्व सोंपा गया था। 100 एकड़ क्षमता तक के तालाब एवं स्टॉप डैम के निर्माण का दायित्व भी कृषि विभाग को सोंपा गया था। तब से लगाकर वर्ष 2012 तक कृषि विभाग द्वारा विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं, जैसे विश्व बैंक की सहायता से संचालित परवानाला जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना,नदी घाटी बाढ़ उन्मुख नदी योजना, राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना, माइक्रो मैनेजमेंट योजना एवं डेनिडा की सहायता से संचालित जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना आदि का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जाता रहा।
2013 आते-आते इन गतिविधियों पर विराम लग गया और सिंचाई संबंधी तमाम योजनाएं क्रियान्वित करने का दायित्व जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया।
इसमें दो मत नहीं कि कृषि, प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, लेकिन सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने संबंधी तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन में लेतलाली, विभागीय अमले की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है।
उदाहरणार्थ ,वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई थी। इसके एक घटक ‘हर खेत को पानी’ का क्रियान्वयन प्रदेश में नगण्य है। राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र विकास मिशन की गतिविधियां भी गैर तकनीकी अमले के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।
इन परिस्थितियों में योजनाओं से वांछित परिणाम मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
यद्यपि स्थिति विकट है, लेकिन भूमि एवं जल संरक्षण नीति में आवश्यक प्रावधान कर हल निकाला जा सकता है।
सर्वप्रथम तो नीति में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कृषक को सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था नहर,लघुत्तम सिंचाई योजना,सामुदायिक नलकूप, स्टाप डैम अथवा उद्वहन सिंचाई आदि जो भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो,के माध्यमों से की जा सकती है।
सिंचाई कृषि का एक आवश्यक अंग है,अतः इससे संबंधित योजनाओं में कृषि विभाग का दखल भी उपयोगी साबित हो सकता है। पूर्व में कृषि विभाग भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर चुका है।
प्रदेश में भूमि एवं जल संरक्षण गतिविधियों के एकीकृत रूप से सुचारू संचालन के लिए ‘भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड’ की स्थापना की जा सकती है, अथवा संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास में पृथक से एक अनुभाग की स्थापना की जा सकती है।
वर्षा ऋतु के समय सतह पर एवं छोटे बड़े नालों में व्यर्थ बहने वाले जल को रोकने एवं उसके उचित प्रबंधन के लिए राज्य योजना मद से एक नई योजना ‘मिशन ऑन ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट ऑन वाटरशेड बेसिस’ भी क्रियान्वित की जा सकती है।
प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों से हर वर्ष कृषि अभियांत्रिकी स्नातक निकल रहे हैं,जिनका उपयोग भूमि एवं जल संरक्षण गतिविधियों में किया जा सकता है।
कैसी विडंबना है कि स्पष्ट नीति के अभाव में एक ओर तो युवाओं को उनकी शिक्षा के अनुरूप नौकरियां नहीं मिल रही हैं,दूसरी ओर तकनीकी काम गैर तकनीकी अमले से कराया जा रहा है।
इसके पहले कि जल संकट विकराल रूप ले, आवश्यकता है,जल संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन की। जल संरक्षण संबंधी परंपरागत विधियों के साथ-साथ उपयोगी नवाचारों को अपनाने की,और उपलब्ध विशेषज्ञता के बेहतर इस्तेमाल की।
*आशुतोष श्रीवास्तव
(लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं।)