अथर्ववेद के कांड 12 का सूक्त 1 जिसके ऋषि अथर्वा हैं और देवता पृथिवी है, वेद के दर्शन, काव्य और विराट मानवीय आदर्श का एक सार्वकालिक और सार्वभौमिक प्रतिनिधि आलेख है जो विश्व-सहित्य की अमूल्य धरोहर है । आश्चर्यजनक रीति से इसमें आज का विज्ञान और पर्यावण का चिन्तायुक्त वह सामाजिक सरोकार भी सम्मिलित है जिसका समाधान विश्व स्तर पर लगातार खोजे जाने की चेष्टा चल रही है ।
हम कह सकते हैं कि पृथिवी सूक्त पर्यावरणीय संतुलन का वह शाश्वत संदेश है जो अजस्रतः सर्वदेशीय है ।
वर्तमान में हम पृथिवी की आराधना तो दूर उसकी रक्षा के लिए भी प्रस्तुत नहीं हैं। पृथिवी के संसाधनों का अपनी विलासिता के लिए जितना परिशोषण आज हो रहा है इतना इसके पूर्व कभी किए जाने की परिकल्पना भी कठिन प्रतीत होती है । वनस्पति और जल का अप्रत्याशित दोहन, वनों का संहार, कृत्रिम वातानुकूलता, उद्योगों की दूषित वायु के उत्सर्जन और अत्यधिक ऊष्मीकरण से ओजोन पर्त भी क्षीण हो चली है ।
दुनियां की आबादी का दिन प्रतिदिन बढ़ता घनत्व, सृष्टि संहारक परमाणु शस्त्रों का अपरिमापित विस्तार और आतंक की छाया में पलती जीवन चेतना की धरती की आयु कितनी और शेष बची है-यह प्रश्न बहुतों के मन में उठ रहा होगा । अभी तक मनुष्य ऐसी कोई वैकल्पिक भूमि की खोज भी नहीं कर पाया है जिस पर उसका पुनर्वास संभव हो सके । यदि लाख और करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर कोई रहने योग्य ग्रह पिण्ड मिल भी जाता है तो कितने लोगों को उसमें विस्थापन मिल सकता है, यह कल्पना का विलास ही समझ आता है । आखिर जिस मजबूती और प्रत्याशा से हम अपना घर बनाकर उसकी रखवाली करते हैं, क्या उसी तीब्रता और संनिष्ठा से सबके घर इस धरती को बनायें रखना हमारा कर्तव्य नहीं है?
यह घ्यान दिए जाने योग्य है कि ऋषि जब पृथिवी से कुछ मांगता है तो उसका यह एक प्रकार का कृतज्ञता बोध है । पृथिवी जब बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा के हमें निरन्तर दिए ही जा रही है तो उसके प्रति एक स्वभाविक अहोभाव की हमारी प्रतीति उससे हमारी प्रगाढ़ता को निरन्तरता देती है । क्या इसमें कोई बाधा भी आती है? इसका शमन कैसे संभव है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए ऋषि का संकेत है कि हमारी चैतन्यता बनी रहना आवश्यक है । हमें निद्रा, तन्द्रा, आलस्य और प्रमाद से ऊपर उठना होगा । प्रत्येक वर्णाश्रयी चाहे वह विद्वान् हो अथवा शूर या कि व्यवशायी, इस पृथिवी से अपनी आवश्यकता की वस्तु इसी अवस्था में प्रचुरता से प्राप्त करता है । ऐसी धरती से वेद का ऋषि प्रार्थना करता है कि ऐसी उदार धरित्री हमें इन सभी क्षेत्रों में ऐश्वर्य प्रदान करे-उक्षतु वर्चसा (12-7) ।
पंच महाभूतों की स्थिति के संबंध में यह शास्त्रोक्त सिद्धान्त सर्व विदित है कि पृथिवी का आधार जल, जल का आधार अग्नि, अग्नि का आधार वायु और वायु का आधार अंतरिक्ष है । यह विवेचन भी महत्वपूर्ण है कि पृथिवी को अंतरिक्ष में गतिमान (विचरन्शील) बताकर वेद के ऋषि ने आज के विज्ञान की खोज के कितने पहले ग्रह पिण्डों के गुरुत्वाकर्षण से संचालित होने की वैज्ञानिकता को प्रतिपादित नहीं कर दिया है!
धरती ही हमारी अन्नदाता है। यह उपकार वह स्वतः सहज रीति से करती जाती है। हमारे बोये बीज कितनी मात्रा में कितनी देर में उपजें, शायद इस अभीप्सा की पूर्ति की सामर्थ्य भी उसके पास है। इसी लिए ऋषि अथर्वा प्रार्थना करते हैं-
‘यत् ते भूमे बिखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु’
(भूमि, तुझमें बीज जो बोयें / बहुत जल्दी उगें!)
आज जब रासायनिक उर्वरकों और प्लास्टिक कचरे से धरती के सीने को पाट दिया गया है, तब इस प्रार्थना की सारवत्ता विचारणीय हो जाती है।
स्टाकहोम और रियो में विश्व के पर्यावरण संबंधी चिंता प्रकट किये जाने के हजारों साल पहले भारत ने मानव के इस नैतिक दायित्व को अच्छी तरह से पहचान लिया था।
अथर्ववेद का पृथिवी सूक्त पर्यावरण की इस आवश्यकता को बड़ी प्रबलता से रेखांकित करता है। इसमें वैदिक ऋषि भावी पीढ़ी की समयोचित आवश्यकता को पर्याप्त पूर्व सम्पूर्णता से प्रकट कर देता है।
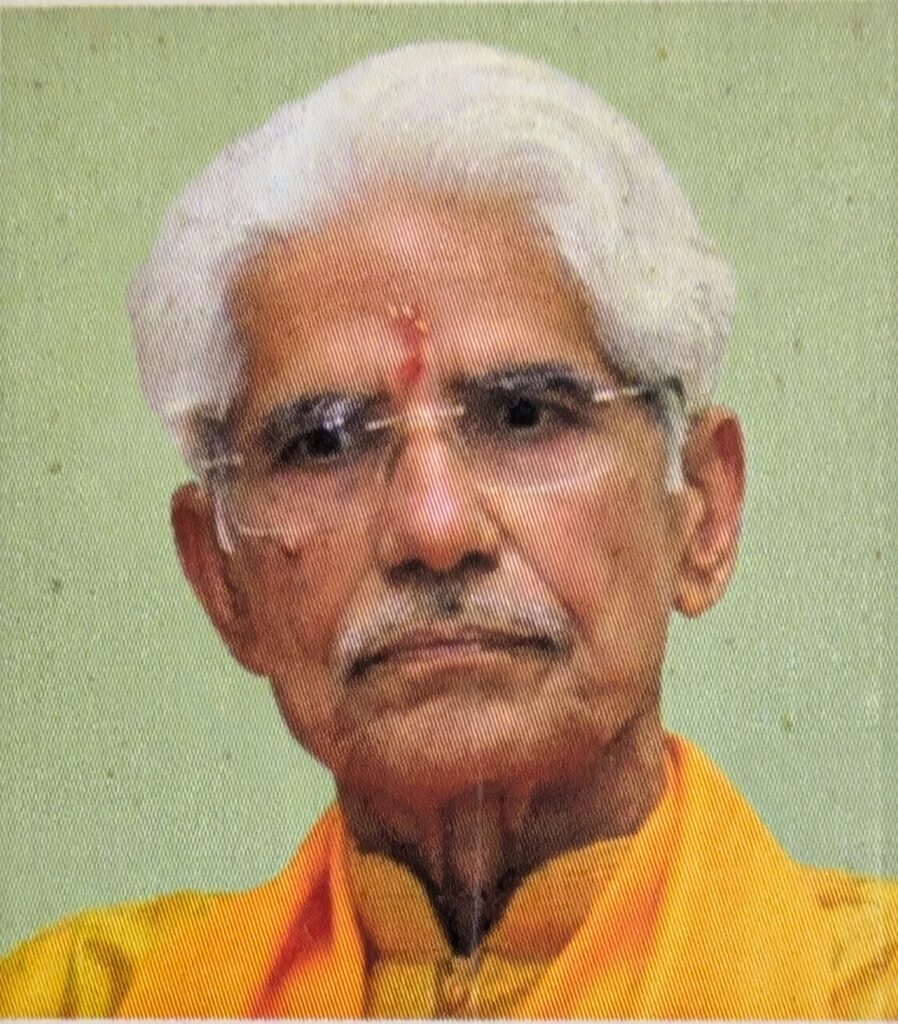
अथर्ववेद के बारहवें कांड के प्रथम सूक्त का नाम पृथवी सूक्त है । इसके दृष्टा ऋषि अथर्वा हैं ।इस सूत्र में कुल ६३ मंत्र हैं।इन मंत्रों में मातृभूमि के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति का परिचय ऋषी ने दिया है।ऋषि ने इस सूक्त में पृथ्वी के आधिभौतिक और आधिदैविक दोनों रूपों का स्वतन किया है।
तासु नो धेह्यभि न: पवस्व माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या:।
पर्जन्य: पिता स उ न: पिपर्तु।
हे पृथ्वी! तुम्हारा जो मध्य स्थान तथा सुगुप्त नाभिस्थान एवं तुम्हारे शरीर संबंधी जो पोशक अन्नरसादि पदार्थ हैं, उनमें हमें धारण करो और हमें शुद्ध करो। भूमि हमारी माता है ,हम पृथिवी के पुत्र हैं। मेघ हमारे पिता अर्थात पालक हैं, वे हमारी रक्षा करें।















