आंध्र प्रदेश की 17 वर्षीय नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा प्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने अपनी टिप्पणी में कहा – छात्रों की आत्महत्या शिक्षा व्यवस्था की ‘संस्थागत असफलता’ है।
इसका सीधा सा अर्थ है,संस्थाएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही हैं।संस्थागत संवेदनहीनता, अकादमिक दबाव और असफलता को संभालने जैसे मुद्दों की अनदेखी छात्रों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने की वजह बन रही हैं।
इसकी रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देशभर के स्कूल,कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों के लिए 15 दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक संसद या राज्यों की विधानसभाएं इस पर कानून नहीं बनातीं ,यह दिशानिर्देश शिक्षण संस्थानों के लिए बाध्यकारी होंगे।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशानुसार –
जिस संस्थान में 100 से अधिक छात्र-छात्राएं होंगे वहां प्रशिक्षित सलाहकार अथवा इस क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त करना होगा।
शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति (जिसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने का समयबद्ध लक्ष्य रखा गया है) के प्रावधानों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य नीति अपनानी होगी।
कोचिंग संस्थानों में प्रदर्शन पर आधारित अलग-अलग समूह नहीं बनाए जाएंगे। इससे शेष छात्रों को शर्मिंदगी होती है।
संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, अस्पतालों आदि के हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं।
परीक्षा अथवा कोर्स बदलाव के तनाव से निपटने के लिए छात्रों को मैंटर या परामर्शदाता उपलब्ध कराए जाएं।
संस्थान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मानसिक तनाव से जूझ रहे अथवा कमजोर वर्गों के छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो।
भेदभाव अथवा यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों के लिए संस्थान स्तर पर समिति का गठन हो जिसके माध्यम से पीड़ित छात्रों को सहायता और सुरक्षा मिले।
संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वह आत्महत्या की प्रवृत्ति अथवा संकेतों को समझ सकें।
संस्थान प्रतिवर्ष परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित प्रतिवेदन बनाकर नियामक संस्था को उपलब्ध कराएं।
अभिभावकों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि वह अपने बच्चों में तनाव के लक्षण पहचान सकें और उन पर अनावश्यक दबाव न बनाएं।
छात्रों और अभिभावकों के लिए नियमित कैरियर परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो उनकी रुचि के अनुसार विषय और कैरियर चयन करने में सहायता करे।
परीक्षा पद्धति हर दृष्टि से छात्रों के हित में हो। नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास पर पर भी ध्यान दिया जाए।
बड़े कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर की जा रही कार्यवाही की जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नियमित एवं निरंतर निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
यह सुनिश्चित करना हाॅस्टल संचालक की जिम्मेदारी है कि परिसर नशा,हिंसा अथवा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से पूर्णतः मुक्त हो।
हॉस्टल संचालकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हॉस्टल के पंखे,छत एवं बालकनी जैसी जगहों पर सुरक्षा उपकरण लगे हों, ताकि आत्महत्याओं को रोका जा सके।
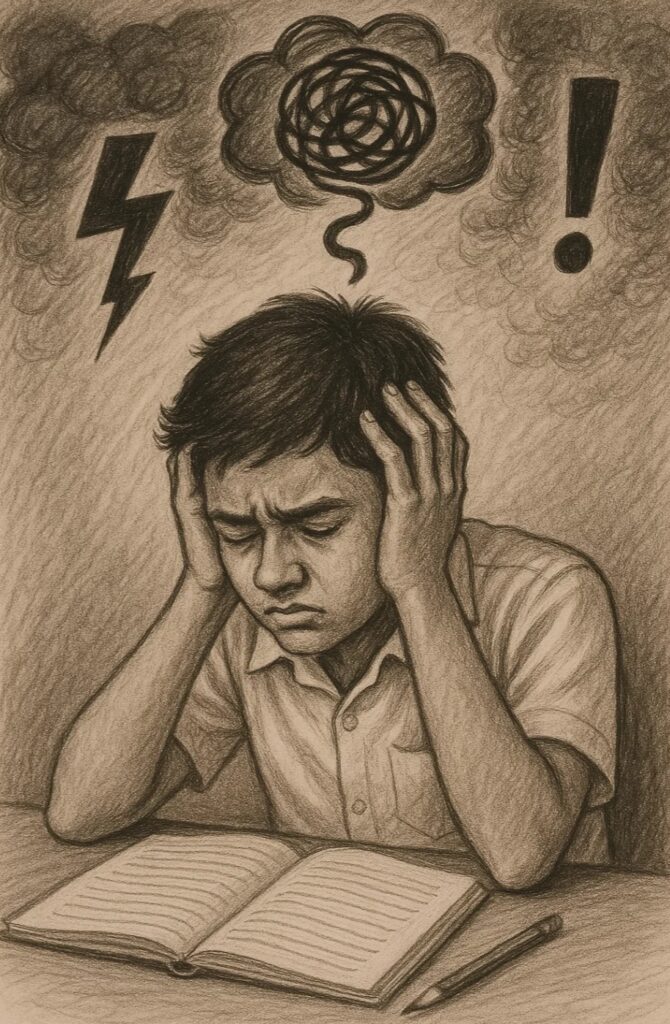
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 13044 छात्रों द्वारा आत्महत्या की गई थी। इनमें से 2248 मौतों के लिए सीधे तौर पर परीक्षा में असफलता को जिम्मेदार माना गया।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अब इस संकट की और अनदेखी नहीं की जा सकती।
न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि वह कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुपालन, छात्रों की सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के संबंध में 90 दिनों के भीतर न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी होने के उपरांत हो सकता है सरकारें इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं।
दरअसल देश में एक अजीबोगरीब रिवाज़ चल पड़ा है। जनकल्याणकारी शासन प्रणाली में जो काम सरकार को सहज रूप से करना चाहिए,उनके लिए भी न्यायालयों को आदेश जारी करना पड़ते हैं, जबकि सरकारी अमला सामान्यतः दुर्घटना घटित होने के बाद ही सक्रिय होता है।
शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों के संचालन संबंधी दिशानिर्देश तय करना और उन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया पहल को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि सरकारें शैक्षणिक परिसरों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सकारात्मक वातावरण सृजित करने के प्रति उदासीन रही हैं। सरकार इस आक्षेप से भी नहीं बच सकती कि उसकी उदासीनता के चलते कोचिंग संस्थान ज्ञान केंद्र नहीं बल्कि व्यवसायिक केंद्र बनकर रह गए हैं।
*अरविन्द श्रीधर















