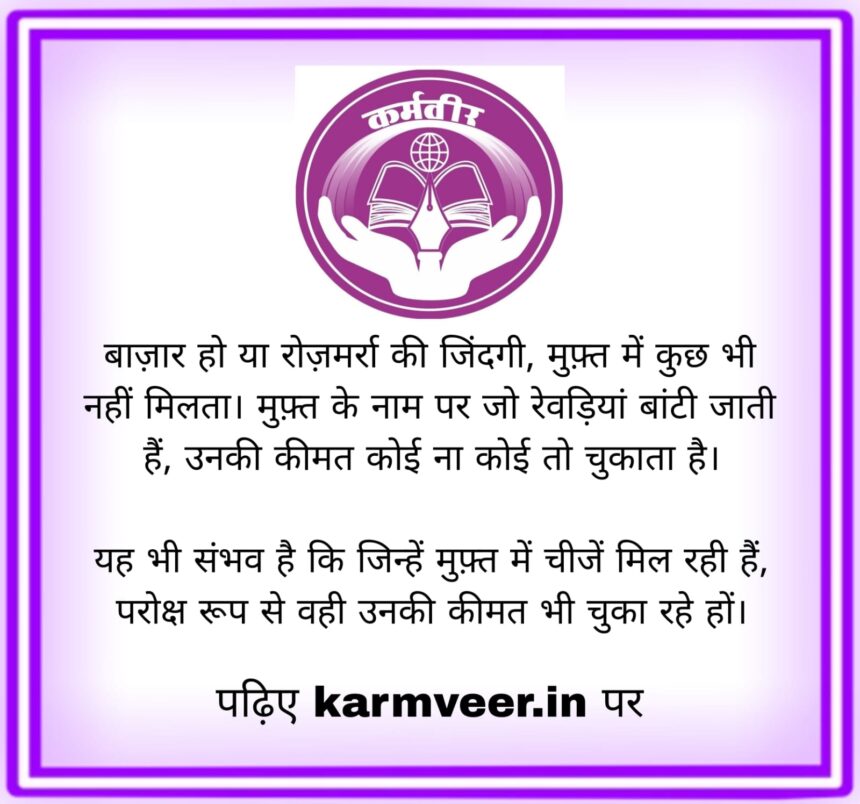सोशल मार्केटिंग (सामाजिक विपणन) की एक सामान्य सी अवधारणा है कि लोग मुफ़्त में मिली चीजों की कद्र नहीं करते।
दूसरी अवधारणा यह कि विज्ञापन सृजित मायाजाल में उलझ कर जब लोग शराब,सिगरेट और अन्य हानिकारक उत्पाद खरीद सकते हैं,तो लक्षित समूह के लिए विशिष्ट विज्ञापन रणनीति के माध्यम से उन्हें जीवनोपयोगी चीज़ों के दाम चुकाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है।
तीसरी सामान्य सी अवधारणा के अनुसार बाज़ार हो या रोज़मर्रा की जिंदगी, मुफ़्त में कुछ भी नहीं मिलता। मुफ़्त के नाम पर जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं, उनकी कीमत कोई ना कोई तो चुकाता है।
यह भी संभव है कि जिन्हें मुफ़्त में चीजें मिल रही हैं, परोक्ष रूप से वही उनकी कीमत भी चुका रहे हों।
ऐसा नहीं है कि यह तीनों बातें कोई गूढ़ रहस्य हैं, जिन्हें समझना सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं है। साधारण से साधारण आदमी भी इन बातों को समझता है। लेकिन आश्चर्य है कि इसके बाद भी देश में चारों तरफ फ्रीबीज अथवा मुफ़्त की रेवड़ियां बांटने वालों की दुकानें सजी हुई हैं।बांटने वाले आनंद में हैं तो पाने वाले परमानंद में।
राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए। शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार,कृषि आदि बुनियादी आवश्यकताओं संबंधी नई योजनाएं बराय नाम नज़र आती हैं,जबकि रेवड़ियों का उल्लेख प्रमुखता से किया जाता है। राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर होड़ मची हुई है कि कैसे अपनी रेवड़ी योजनाओं को प्रतिपक्षी की योजनाओं से अधिक मीठा और आकर्षक बनाया जाए।
मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई लाड़ली बहना योजना ने तो जैसे परिदृश्य ही बदल कर रख दिया है। राजनीतिक दल चाहे क्षेत्रीय हों अथवा राष्ट्रीय,सभी में इस योजना को अपना बनाने की होड़ लगी है। हर कोई इसे और आकर्षक बनाकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहता है।
मजे की बात यह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी योजनाओं को तो जनकल्याणकारी बताते हैं, जबकि दूसरे दल की वैसे ही योजनाओं को मुफ़्त की रेवड़ी कहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2015 में चुनाव आयोग ने फ्रीबीज को लेकर एक आचार संहिता जारी की थी, लेकिन वह प्रभावी साबित नहीं हुई।
किस योजना को फ्रीबीज कहा जाए और किसे जनकल्याणकारी, इस संबंध में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
दरअसल नियम कायदे कानूनों को अपनी सुविधा के अनुकूल ढाल लेना हमारी फितरत बन गई है।
शोषित वंचित गरीबों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाना सरकार का दायित्व है,लेकिन इसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है उसे केवल जनकल्याण का भाव तो नहीं कहा जा सकता।
ऐसा नहीं है कि चुनावों के समय मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रारंभ की गई हर योजना फ्रीबीज ही साबित हुई हो। कुछ ऐसी भी चुनावी घोषणाएं रही हैं जो आगे चलकर राष्ट्रीय फलक पर लोकप्रिय और उपयोगी साबित हुईं।
1960 के दशक में तमिलनाडु से प्रारंभ हुई मिड डे मील योजना न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई, अपितु इसके कारण स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में भी इज़ाफ़ा हुआ।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामा राव ने फ्री राशन योजना के तहत 2 किलो चावल मुफ्त देना प्रारंभ किया था। वर्तमान में नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम पूरे देश में लागू है।
2018 में तेलंगाना में “रायथू बंधु” योजना के तहत किसानों को सालाना ₹10000 की मदद प्रारंभ की गई थी जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया।
फ्रीबीज की वर्तमान प्रचलित राजनीति का प्रारंभ भी तमिलनाडु से ही माना जाता है। 2006 के विधानसभा चुनाव के दौरान डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में फ्री कलर टीवी देने का वादा किया था। सरकार बनने पर इस वादे को पूरा करने के लिए खजाने से 750 करोड रुपए खर्च किए गए।
अन्नाद्रमुक कहां पीछे रहने वाली थी। 2011 के विधानसभा चुनाव में उसने मतदाताओं को मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप,कंप्यूटर आदि बांटने का वादा कर दिया। इसके साथ-साथ विवाह के समय महिलाओं को ₹50000 और राशन कार्ड धारकों को 20 किलो चावल देने का वादा भी किया गया। जाहिर है,इस बार सरकार अन्नाद्रमुक की बनी।
इसके बाद तो जैसे फ्रीबीज चुनावी रणनीति का प्रमुख हथियार ही बन गया। अब तो लोगों को इंतजार रहता है कि चुनाव आएं और उन्हें पिछली बार से कुछ अधिक हासिल हो। हालांकि यह इस बात का संकेत भी है कि राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों से कहीं अधिक फ्रीवीज पर भरोसा है।
पता नहीं यह होड़ कहां तक जाएगी?
देश को जनकल्याणकारी कार्यक्रम और फ्रीबीज के अंतर को समझना होगा। जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है।
इसे साधारण भाषा में कुछ इस तरह से कह सकते हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरवारों को घर देना जनकल्याणकारी है,लेकिन झुग्गी बसाहट को प्रोत्साहित करना समाज और राष्ट्र दोनों के लिए अहितकर है। रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम देना जनकल्याणकारी है,जबकि घर बैठे गैर जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध करवाना उन्हें अकर्मण्य बनाना है। हर गली और घर प्रकाशित हो, यह जनकल्याणकारी गतिविधि है, लेकिन मुफ्त बिजली प्रदाय के चक्कर में तमाम बिजली कंपनियां घाटे में चली जाएं, यह शुभ लक्षण नहीं है।
हम 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। इसके लिए भौतिक संसाधनों के साथ-साथ सबल,समर्थ एवं समर्पित नागरिकों के सक्रिय समर्थन की भी आवश्यकता होगी। यदि हम जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के बजाय फ्रीबीज के जरिए ऐसे नागरिक गढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो माफ करिए हम गलत दिशा में जा रहे हैं।
*अरविन्द श्रीधर