संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।
शासन तंत्र के तीनों अंग सुचारु रुप से कार्य कर सकें इसके लिए अधिकारियों,कर्मचारियों,विशेषज्ञों की लंबी-चौड़ी फौज भी होती है। सामान्यतः इन्हें लोक सेवक अथवा नौकरशाह कहा जाता है। यही वह वर्ग है जिसके माध्यम से विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।कार्यपालिका द्वारा निर्धारित जनकल्याणकारी योजनाएं लागू होती हैं एवं न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसलों अथवा व्यवस्थाओं पर कार्यवाही सुनिश्चित होती है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना भी इसी वर्ग की जिम्मेदारी है।
कार्यक्षेत्र के इतने स्पष्ट विभाजन के बावजूद देखने में आता है कि चाहे आम नागरिक हों,विभिन्न शासकीय-अशासकीय संस्थाएं हों,अथवा स्वयं सरकारें ही क्यों ना हों,हर छोटे-बड़े मामले में अदालती समाधान की ही अपेक्षा रखते हैं।
यद्यपि यह चलन न्यायपालिका की निष्पक्षता और आम नागरिकों के देश की अदालतों पर दृढ़ विश्वास का परिचायक है,लेकिन संविधान सम्मत शक्ति संतुलन की दृष्टि से यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। यह चलन एक तरह से जिम्मेदार संस्थाओं की अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने की प्रवृत्ति की ओर भी इशारा करता है।
ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति,प्रशासनिक दृढ़ता और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका अपनी संविधान सम्मत भूमिका का निर्वहन कर सकती थी, लेकिन उसने अवसर गवां दिए।
कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे आसानी से समझा जा सकता है।
सर्वविदित है कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती,लेकिन सरकारें ऐसा करती हैं।ऐसे अनेक मामले सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।
ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल संविधान द्वारा आरक्षण के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के बारे में नहीं जानते हैं।अच्छी तरह से जानते हैं,लेकिन इस पूरी कवायद का उद्देश्य होता है लक्षित आबादी तक उनके हित चिंतक होने का संदेश पहुंचाना और राजनीतिक बढ़त हासिल करना।
यही स्थिति क्रीमी लेयर के आरक्षण को लेकर भी बनती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से कह चुका है – ‘यह तय करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है कि जिन लोगों ने कोटा का लाभ लिया और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ गए,उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए या नहीं?’
संविधान पीठ यह भी कह चुकी है कि ‘अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार भी राज्यों के पास है। उन्हें ही यह तय करना चाहिए कि कौन सी जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं।’
ऐसा ही एक मामला है,यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान से संबंधित। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। 2004 से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर अदालती कार्यवाही चल रही है। जैसे-तैसे 3 दिसंबर 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट ने कचरा निस्तारण करने का आदेश दिया। इसके पहले कि अदालती आदेश के परिपालन में कचरे का निस्तारण हो पाता, मामला एक बार पुनः राजनीतिक दुष्चक्र में उलझ गया।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गठित तमाम समितियों,टास्क फोर्स और विशेषज्ञों की लंबी चौड़ी फौज के होते हुए भी 40 सालों तक समस्या का हल ना हो पाना,क्या जिम्मेदारों की नाकामी नहीं है।
18 फरवरी 2025 को एक बार फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जहरीले कचरे के चरणवद्ध निस्तारण का निर्देश दिया है।
यह भी उल्लेखनीय है कि जहरीले कचरे को चरणबद्ध तरीके से नष्ट करने की लगभग पूरी प्रक्रिया भी अदालत द्वारा ही निर्धारित की गई है।
शासन-प्रशासन द्वारा जो कदम अदालती निर्देश के बाद उठाए गए हैं, क्या पहले नहीं उठाए जा सकते थे?
बिल्कुल उठाए जा सकते थे,लेकिन स्थानीय विरोध के चलते जिम्मेदार लोग एक बार फिर पीछे हट गए ताकि फैसले का ठीकरा उनके सिर पर न फूटे।
देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। टी एन शेषन के समय देश निर्वाचन आयोग की शक्तियां देख चुका है। लेकिन फिलहाल हालत यह है कि आयोग फ्रीबीज पर पॉलिसी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रीबीज को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा चुकी है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के मामले में भी जिम्मेदारों की नाकामी सिद्ध हुई है। जबकि सर्वोच्च अदालत इस संबंध में भी स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुकी है।
जनहित याचिकाओं के कारण इस प्रवृत्ति में और भी अभिवृद्धि हुई। इस व्यवस्था से जहां एक ओर शोषित-वंचित लोगों को उनका हक मिला,वहीं दूसरी ओर पेशेवर याचिका कर्ताओं की वजह से इस व्यवस्था का दुरुपयोग भी सामने आया। कई बार तो याचिका कर्ताओं को फटकार भी पड़ी।
इसके पीछे भी कहीं ना कहीं नौकरशाही की लेतलाली ही समझ में आती है। आखिर लोक सेवकों की लंबी चौड़ी व्यवस्था के होते हुए किसी भी नागरिक को जनहित याचिका की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए?
मामला चाहे सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का हो अथवा सार्वजनिक हित के लिए भूमि अधिग्रहण का,शासकीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों का हो अथवा स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव में हुई गड़बड़ी का, उत्तरदायी अधिकारियों का प्रयास होता है कि इस संबंध में अदालत का कोई निर्देश आ जाए तो उनकी राह आसान हो।
कई बार तो निर्णय लेने में टालमटोल सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि संबंधित पक्ष अदालत में चला जाए और उनकी जान छूटे।
जिम्मेदार संस्थाएं ऐसे फैसले लेने से बचती हैं जो कठोर प्रकृति के हों अथवा अलोकप्रियता का कारण बन सकते हों।
स्पष्ट है ,अदालतों का उपयोग अपनी खाल बचाने के लिए किया जा रहा है।
यह भी एक विडंबना है कि एक ओर तो हर छोटे-बड़े मामले में न्यायिक समाधान की प्रवृत्ति बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका पर न्यायिक सक्रियता और न्यायिक हस्तक्षेप के आरोप लगाए जाते हैं।
धर्म क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। यहां भी आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए अदालती लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च माना जाता है। इस पद पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परम ज्ञानी एवं वीतरागी संन्यासी ही प्रतिष्ठित होते है।
विचारणीय है कि एक ही पीठ पर शंकराचार्य पद के दो दावेदारों में से कौन वास्तविक अधिकारी है, इसका फैसला भी विद्वत समाज नहीं कर पा रहा।मामला अदालत में विचाराधीन है।
ठीक है,अदालती फैसले निष्पक्ष होते हैं और प्राय: सभी पक्ष फैसलों का सम्मान भी करते हैं,लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि जो फैसले कायदे- कानूनों के दायरे में सामान्य प्रक्रिया के तहत लिए जा सकते हों,उनके लिए अदालतों का कीमती वक्त जाया किया जाए।अदालतें वैसे भी अनिर्णीत मुकदमों के बोझ से दबी हुई हैं। ऐसे में शासन तंत्र के अन्य अनुभागों का काम भी उनके पाले में डालना कहां तक उचित कहा जा सकता है?
भारतीय नौकरशाहों बारे में यह विख्यात है कि उन्हें किसी समस्या के समाधान के उपाय भले ही ज्ञात न होते हों, यह भली भांति ज्ञात होता है कि साधारण सी समस्या को नियम-कायदों के जाल में उलझाकर जटिल कैसे बनाया जा सकता है।
इस छवि को तोड़ने का एक ही उपाय है कि ब्यूरोक्रेसी अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाए। अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए उसके पास पर्याप्त अधिकार हैं,जो कायदे कानूनों से संरक्षित हैं। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन अधिकारों के निष्पक्ष प्रयोग की।
यदि ऐसा हो सका तो न्यायपालिका का बोझ तो कम होगा ही,त्वरित न्याय की राह भी आसान होगी।
*अरविन्द श्रीधर










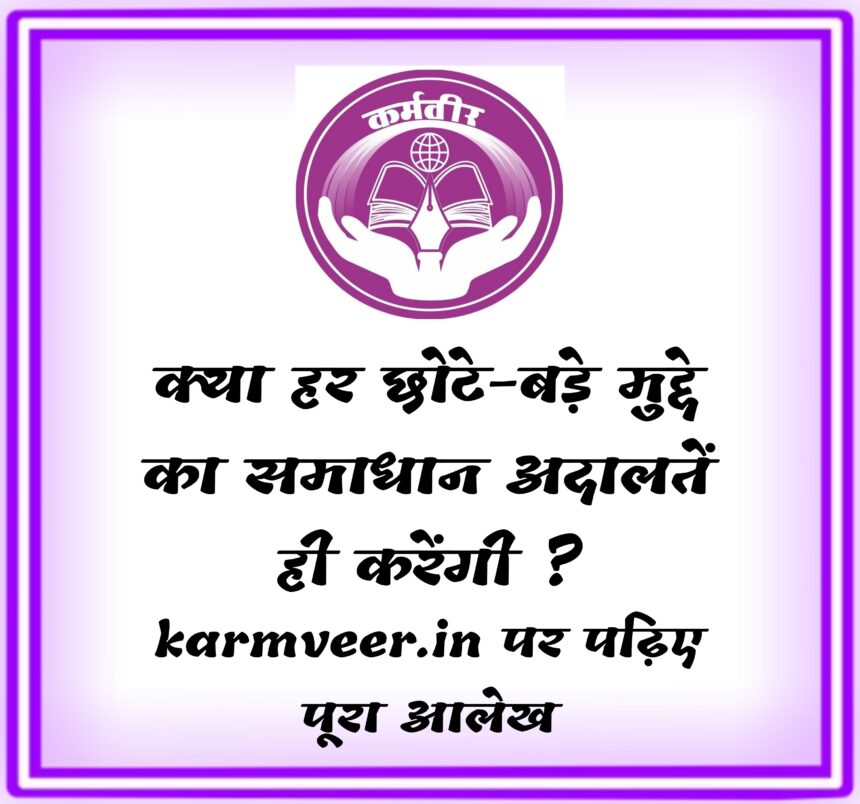





विचारोत्तेजक आलेख… हार्दिक बधाई 🌹🌹