संविधान के प्रावधानों से इतर लोकमानस में चौथे स्तंभ के तौरपर स्थापित प्रेस आज भी अन्य स्तंभों से ज्यादा विश्वसनीय, सहज और सुलभ है। समस्याओं से घिरा आम आदमी सबसे पहले अखबार के दफ्तर में जाकर फरियाद करता है। थाने, दफ्तरों और भी सरकरी गैर सरकारी जगहों में जब वह दुरदुराया जाता है तो उसका आखिरी ठिकाना भी प्रेस का ही दफ्तर होता है। यह छपे हुए शब्दों की ताकत है जो प्रेस को तमाम लानतों मलानतों के बावजूद प्रभावी बनाए हुए है।
बहुत सी धारणाओं की स्थापना लोकमानस के जरिये होती है। जैसे प्रेस का मतलब आज भी अखबार और पत्रिकाएं हैं न कि टीवी चैनल और बेव पोर्टल। इसलिए प्रेस के समानांतर ‘मीडिया’ के नाम को चलाने के जतन शुरू हुए लेकिन प्रेस शब्द का रसूख कायम है। इस शब्द को अभी भी ऐसा उच्च सम्मान प्राप्त है कि अपराधी भी प्रायः इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। कमाल की बात है कि जिस ‘प्रेस’ शब्द को भारतीय संविधान ने अपने पन्नों में भी जगह नहीं दी उसे लोक मानस ने आगे बढ़कर सिरोधार्य किया।
अस्सी के दशक के शुरुआती वर्षों में जब टेलीविजन आया तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अखबारों के दिन गए। प्रेस के भविष्य पर गंभीर चर्चाएं शुरू हुईं। लेकिन टीवी का आना फायदे का ही साबित हुआ। अखबार ज्यादा सतर्क हुए। रंगीन होने का दौर शुरू हुआ। लेआउट्स और प्रोडक्शन की दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। बड़े घरानों से लेकर मध्यम दर्जे तक के अखबार प्रतिष्ठानों में आर एंड डी( रिसर्च एन्ड डवलपमेंट) के विभाग खुले।
अस्सी के दशक को आप प्रेस का सुनहरा दौर कह सकते हैं। खुफिया कैमरे, और बटन रिकार्डर नहीं थे फिर भी एक के बाद एक सनसनीखेज खोजी रिपोर्ट्स आईं जिनकी नजीर आज भी दी जाती है।
रविवार, दिनमान, माया, इलुस्ट्रेटेड वीकली, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं दैनिक अखबारों से लोहा लेने लगी। अखबार और पत्रिकाओं में आगे निकलने की कड़ी स्पर्धा शुरू हुई। इस दशक में रिकॉर्ड तोड़ पाठक बढ़े और उसी हिसाब से नए अखबार और जमे-जमाए अखबारों के संस्करण। दूरदर्शन काला- सफेद से रंगीन हुआ। दर्शक जीवंत खबरें देखने लगे। टीवी अखबारों के लिए कैटलिस्ट साबित हुआ। पढ़ने की भूख जगी। यह प्रेस पर पाठकों की कृपा है, ये इज्जत, शोहरत, ताकत लोक की वजह से है सरकार की वजह से नहीं, यह बात अच्छे से समझ लेना चाहिए।
छपे हुए शब्द आज भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय और खरे हैं। हाल ही की एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि पाठकों का भरोसा मुद्रित माध्यमों के प्रति और बढा है। 1990 के बाद निजी क्षेत्र के चैनल आए। खबरों की बड़ी.स्पर्धा शुरू हुई। विदेशी चैनलों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए। एक बार फिर इस जनसंचार क्रांति से ऐसा लगा कि अखबार और पत्रिकाओं का भट्ठा बैठ जाएगा। कुछ शुरुआती असर दिखा भी लेकिन लोकमानस में चैनल्स खबरों को लेकर अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, जबकि ये ऐसे माध्यम हैं कि खबरें जीवंत दिखती हैं।
अब आते हैं प्रेस की स्थिति पर। प्रेस की इस महत्ता ने हर क्षेत्र के व्यवसाइयों को अपनी ओर खींचा है। बिल्डर,चिटफंडिये,खदानों और शराब का ठेका चलाने वाले, राजनीति में रसूख जमाने की लालसा रखने वाले नवकुबेर, प्रेस ने सभी को लुभाया।
प्रेस को पेशेवराना अंदाज से ही चलाया जा सकता है इसलिये मीडिया के पुराने घराने ही इस मैंदान में कायम हैं। वे वो हर तिकड़म जानते हैं कि कैसे उनका रसूख भी कायम रहे और मीड़िया का धंधा भी चलता रहे। 1966 में प्रेस कौंसिल आफ इंडिया के गठन के बाद अखबारों में काम करने वालों के हित में कई वेजबोर्ड बने। तीस साल से बछावत, बेजबरुआ और मजीठिया का नाम सुन रहे हैं, शायद ही किसी मीड़िया घराने ने ईमानदारी से इनकी सिफारिशें लागू की हों। ये सभी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की अध्यक्षता में बने। इन दिनों मजीठिया की सिफारिशों को लागू करने पर जोर है।
प्रायः सभी बड़े मीडिया समूहों ने इसका रास्ता निकाल लिया। अपनी ही आउटसोर्स कंपनियां बना लीं और पत्रकारों को नौकरी छोड़ने या आउटसोर्स कंपनी में काम करने का विकल्प रखा। मजबूरी में पत्रकार ने इसे स्वीकार कर लिया। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के एक बड़े मीडिया समूह से निकाले गए एक पत्रकार की लावारिस मौत सुनकर दहल गया। वह न्याय को लेकर लड़ाई लड़ रहा था। व्यवस्था ने साथ नहीं दिया।
आज की तारीख में सबसे कच्ची नौकरी पत्रकारों की है। वे कल किस वक्त निकाल बाहर कर दिए जाएं इसका पता नहीं। अखबारों में दूसरों के शोषण की बात करने वाला खुद कितना शोषित है कि इसका जिक्र तक नहीं कर सकता। बड़े अखबारों में इस बात की घोषित मनाही है कि वह पत्रकारों की यूनियन से नहीं जुड़ेगा। पत्रकारों की यूनियनें बँटी हुई हैं। श्रम कानूनों को सरकारों ने ही बधिया बनाके रखा है। सो पत्रकार जो दुनिया की नजरों में बड़ा क्रांतिकारी है, घुट घुटकर मरता है।
आँचलिक पत्रकारिता की तो और दुर्गति है। पहले अखबार मालिक उन्हें उतनी ही गंभीरता से लेते थे जैसे बस मालिक अपने.कंडक्टर को। अब तो स्थित यह है कि मामूली से वेतन और विज्ञापन के भारी टारगेट के आधार पर ब्यूरो खोले जाते हैं और जो बैठता है खुद को चीफ कहवा कर ही साँत्वना दे लेता है। इस प्रक्रिया में अपराधियों का तबीयत से पत्रकारीकरण हो गया है। चैनल्स के क्षेत्रीय संवाददाताओं की स्थिति तो और भी गई गुजरी है। इनके हितों की रक्षा कौन करे.? प्रेस कौंसिल.
प्रेस कौंसिल को 1966 में प्रेस के हितों की रक्षा व उन्हें मर्यादित करने के लिए गठित किया गया था। चूँकि 16 नवंबर से उसने काम करना शुरू किया था।इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस घोषित कर दिया। इसके अध्यक्ष अमूमन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। इस संस्था को प्रेस का वाचडाग कहा जाता है। लेकिन इसके रहते ही वो पत्रकार न्याय माँगते हुए बाराखंभा रोड के फुटपाथ में मर गया। यह संस्था कुछ नहीं कर पाई। वह इसलिए कि जिस तरह के अधिकार बार कौंसिल, मेडिकल कौंसिल,टेक्निकल कौंसिल को मिले हैं वैसे अधिकार प्रेस कौंसिल के पास नहीं है।
प्रेस कौंसिल यह भी तय नहीं कर सकता कि किसे पत्रकार कहा जाए किसे नहीं। सबसे बड़ा झगड़ा यह है कि टीवी और डिजिटल मीडिया को प्रेस क्यों माना जाए..! और माना जाए तो प्रेस कौंसिल ने उसे किस तरह परिभाषित किया है इस पर कभी कोई गंभीर विमर्श नहीं हुआ। इस बीच समानांतर मीडिया की भी बात हाशिए से मुखपृष्ठ पर आ गई।
यह ठीक बात है कि सोशलमीडिया ने अखबार वालों की लठैती पर बंदिश लगाई है..या उनके मुकाबले लठ्ठ लेकर खड़े हो गए हैं। सोशलमीडिया के साथ बड़ा खतरा दोधारी तलवार सा है। यदि ये मीडिया के भीतर या समानांतर हैं तो इनको नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था नहीं। प्रेस कौंसिल भी नहीं।
प्रेस कौसिल तो ऐसा नखदंत विहीन वाचडाग है जो सिर्फ भोंक सकता है इससे ज्यादा कुछ नहीं। अखबार मालिकों पर ऐसे भोंकने वालों का कभी असर नहीं पड़ा। हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रेस के साथ ज्यादती की है। प्रेस को अभिव्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना कि एक आम नागरिक का। इस तरह हर व्यक्ति पत्रकार है जो अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करता है। भारत में पत्रकार कोई संवैधानिक शब्द नहीं है।
अमेरिका, यूरोप में ऐसी स्थिति नहीं है। वहां प्रेस संविधान के अनुच्छेद में है और उसकी स्वतंत्राता को चुनौती नहीं दी जा सकती।
हमारे यहां इसकी उलट स्थिति है। क्योंकि पत्रकार की औकात सामान्य नागरिक से ज्यादा कुछ भी नहीं। पत्रकार पर मुकदमा लगता है तो उसे साबित करना होता है कि जो हमने लिखा वो ठीक लिखा। सो प्रेस की आजादी और सुरक्षा की बात करनी है तो संविधान संशोधन कर प्रेस को संविधान के दायरे में लाया जाए। उसका अलग अनुच्छेद बने। और लिखा जाए की प्रेस की स्वतंत्रता को चुनौती नहीं दी जा सकती। वकील,डाक्टर की तरह पत्रकार की न्यूनतम योग्यता तय की जाए। तभी हम भविष्य के प्रेस का कुशल मंगल देख सकते हैं। वरना कितने भी कानून आएं,आयोग और बोर्ड बनें, हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाएं कुछ होना जाना नहीं है।
-जयराम शुक्ल
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

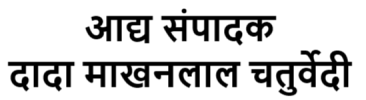
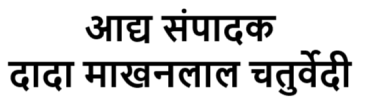

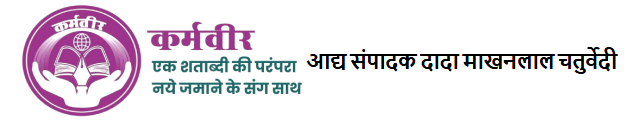


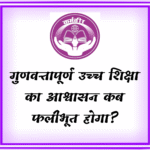








पत्रकारों और प्रेस की मौजूदा स्थिति को दर्शाता बढ़िया आलेख